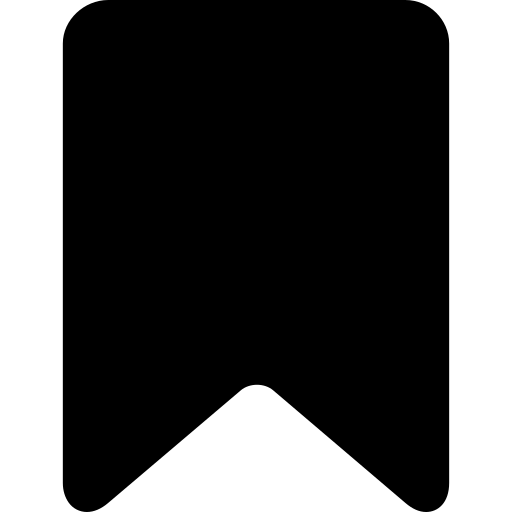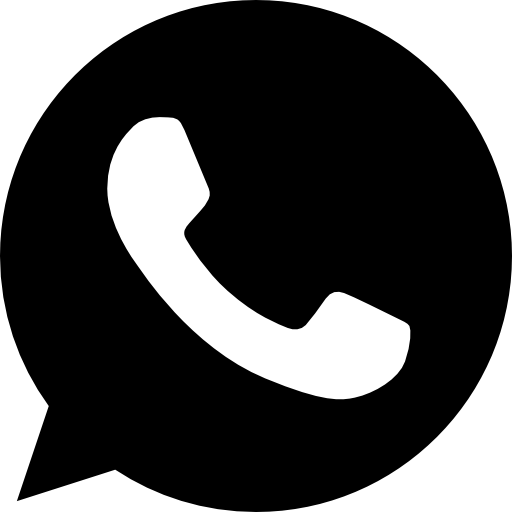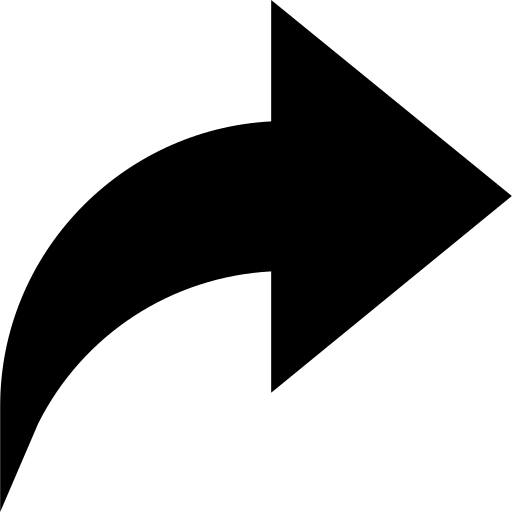भूकंप क्या है? Earthquake Information in Hindi
Earthquake Type, Cause, Facts, Information in Hindi-
दोस्तों आजकल प्रायः हमें भूकंप से संबंधित कई सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं| सन 2015-16 में भारत और उसके आसपास के कई पड़ोसी देशों में भूकंप के कई छोटे और बड़े झटके महसूस किए गए, जिससे लाखों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और इसके साथ ही साथ धन की भी बहुत सारी क्षति हुई| पर क्या आप जानते हैं कि भूकंप क्या है और भूकंप कैसे आते हैं?
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की भूकंप क्या है? भूकंप कैसे आते हैं? और भूकंप आने के क्या-क्या कारण हैं?
भूकंप क्या है? (Earthquake Information in Hindi)–
दोस्तों Earthquake को हम साधारणता भूकंप के नाम से जानते हैं| भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है धरती का कांपना या पृथ्वी का हिलना| जिस प्रकार हम किसी शांत तालाब में यदि एक पत्थर फेंकते हैं तो तालाब के जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगें फैल जाती हैं उसी प्रकार से जब पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल उत्पन्न होती है तो एक जोरदार कंपन उत्पन्न होता है|
यह कंपन पृथ्वी के ऊपरी भाग पर महसूस होता है और हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं| अतः हम यह कह सकते हैं कि भूकंप धरातल के ऊपरी भाग कि वह कंपन क्रिया है जो कि धरातल के ऊपर अथवा नीचे स्थित चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है|
भूकंप के संबंध में सेलिसबरी ने एक परिभाषा दी है और इस परिभाषा के अनुसार भूकंप वे धरातलीय कंपन हैं जो मनुष्य से संबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरुप उत्पन्न होते हैं|
- भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी (Seismology) कहा जाता है|
- अंग्रेजी शब्द ‘सिस्मोलॉजी’ (Seismology) में ‘सिस्मो’ (Seismo) उपसर्ग ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ भूकंप होता है|
- भूकंप विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को भूकंपविज्ञानी कहा जाता है|
- जब भूकंप आता है तो उसके कारण धरातल पर जो कंपन होता है उस कंपनी को हम प्रघात (Shock) कहते हैं|
- भूकंप के उद्गम स्थल को हम उद्गम केंद्र या केंद्र (Center) के नाम से जानते हैं|
- भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर धरती पर स्थित स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र (Epicenter) कहा जाता है|
- समान तीव्रता के भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा के नाम से जानते हैं|
- भूकंप के बाद एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप रेखा कहा जाता है|
भूकंप केंद्र-
पृथ्वी के नीचे जिस स्थान पर भू-खंडीय प्लेटे आपस में टकराती हैं या जहां से आंतरिक संघनित ऊर्जा दरारों भ्रंशो आदि के अनुसार त्वरित कम्पनों को जन्म देती है, उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है|
भूकंपीय तरंगों के प्रकार
भूकंपीय तरंगे चार प्रकार की होती हैं-
प्राथमिक तरंगे-
प्राथमिक तरंगो को प्रधान तरंगो के नाम से भी जाना जाता है| अनुदैर्ध्य तरंगें जिन की गति तीव्र होती है, यह भूकंप केंद्र से कई सौ किलोमीटर तक प्रसारित होती हैं| इन तरंगो को सर्वप्रथम अनुभव किया जा सकता है|
द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगे
अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति के और औसत आयाम के कंपन होते हैं| यह अधिक हानि नहीं कर पाती है| यह तरंगे ठोस चट्टानों से गुजर सकती है|
धरातलीय तरंगे
धरातलीय तरंगे पृथ्वी की सतह के समान्तर प्रवाहित होती इसी कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं| यह पृथ्वी की सतह को अगल-बगल हिलाती है, जिससे बहुत ज्यादा विनाश होता है|
रेलें तरंगें
सबसे अधिक कम्पन इन्ही तरंगों के कारण होता है| यह तरंगें पृथ्वी की सतह पर लुढ़कती हैं|
एक साल में कितने भूकंप आते हैं?
भूकंप मापी यंत्र के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि विश्व के संपूर्ण देशों में 1 साल की अवधि के दौरान लगभग 8000 से 10000 तक भूकंप आते हैं| और इस कारण हम यह कह सकते हैं की पूरे विश्व के किसी न किसी कोने में हर घंटे में एक भूकंप जरूर आता है| भूकंप के कुछ झटके या कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जिनको अभी रिकॉर्ड करना संभव नहीं हो सका है, इस कारणवश हम यह भी कह सकते हैं कि 1 साल में 10000 से भी कहीं ज्यादा भूकंप पूरे विश्व में आते हैं|
विश्व के अधिकांश भूकंप धरती के तल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं|
भूकंप आने के क्या-क्या कारण हैं?
दोस्तों भूकंप आने के कई कारण हैं, और हर कारण से छोटे या बड़े सभी प्रकार के भूकंप उत्पन्न होते हैं| भूकंप आने के कारण अग्रलिखित हैं-
ज्वालामुखी विस्फोट-
भूकंप आने में ज्वालामुखी विस्फोट एक महत्वपूर्ण कारक है जब कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उसके आसपास स्थित क्षेत्रों में एक हलचल उत्पन्न होती है और इस हलचल को हम भूकंप के नाम से जानते हैं| कई बार पृथ्वी के अंदर पल रहे ज्वालामुखी में उपस्थित लावा कण पृथ्वी से बाहर आने का प्रयास करते हैं जिसका विरोध पृथ्वी तल द्वारा किया जाता है और इस कारणवश ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है और शक्तिशाली तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिस कारण से धरती तल पर भूकंप आता है|
पृथ्वी का सिकुड़ना-
भूकंप के आने में पृथ्वी का सिकुड़ना भी एक महत्वपूर्ण कारक है| जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती समय में पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी और धीरे-धीरे यहां ठंडी होती जा रही है| विज्ञान के नियमों के अनुसार हम जानते हैं कि जब भी कोई गर्म वस्तु ठंडी होती है तो वह संकुचित होती है, इसी सिद्धांत के कारण पृथ्वी भी सिकुड़ रही है| पृथ्वी के सिकुड़ने के कारण ही उसके अंदर स्थित चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है जिसके कारण पृथ्वी के तल पर भूकंप आते हैं|
बलन तथा भ्रंश-
वलन तथा भ्रंश का अभिप्राय संपीड़न एवं तनाव से है| संपीडन एवं तनाव के कारण चट्टानों में हलचल उत्पन्न होती है और भूकंप के झटके पृथ्वी तल पर महसूस किए जाते हैं| संपीड़न एवं तनाव के कारण तीव्र गति के भूकंप भी उत्पन्न होते हैं|
भू संतुलन-
ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी “सियाल” तैर रहा है और वह संतुलन की व्यवस्था में होता है, परंतु जब किसी अपरदन या अन्य स्थिति के कारण उसमें विक्षोभ होता है तो सियाल का संतुलन बिगड़ जाता है और जिसके कारण चट्टानों का भी संतुलन बिगड़ जाता है और भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है|
जलीय भार-
दोस्तों हम जानते हैं कि वर्षा एवं नदियों के पानी का सही उपयोग करने के लिए बांध बनाकर जल को कई बड़े बड़े जलाशयों में एकत्रित किया जाता है| और इस एकत्रित जल को आवश्यकता अनुसार नहरों एवं अन्य माध्यमों से दूरदराज के इलाकों में पहुंचाया जाता है, परंतु जब एक ही जगह पर बहुत सारा जल एकत्रित किया जाता है तो उस स्थान के नीचे उपस्थित चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है, जिससे चट्टानों की स्थिति में परिवर्तन होता है और भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है|
कृत्रिम भूकंप
कृत्रिम भूकंप से अभिप्राय उन भूकंपों से है जिनके आने में मनुष्य पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, इस प्रकार के भूकंप बम के फटने के कारण, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के कारण, एवं रेलगाड़ी तथा अन्य भारी वाहनों के कारण आते हैं|
भूकंप की तीव्रता Intensity of Earthquake-
किसी भी स्थान पर भूकंप की तीव्रता उस स्थान पर भूमि में उत्पन्न गति तथा मानव एवं जानवरों पर प्रभाव के रूप में मापी जाती है| अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी भूकंप के द्वारा हुए विनाश को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भूकंप कितना तीव्र था| भूकंप की तीव्रता को मरकेली पैमाने पर मापा जाता है| इस पैमाने को मरकेली पैमाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरकेली ने किस पैमाने को विकसित किया था| मरकेली ने भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने का विकास सन 1902 में किया था| मरकेली के पैमाने को सन 1931 में वुड एवं न्यूमैन ने संशोधित किया था और इस संशोधित पैमाने को हम संशोधित मरकेली पैमाना (Modified Mercalli Intensity Scale.) के नाम से जानते हैं|
भूकंप का परिमाण Magnitude of Earthquake-
भूकंप का परिमाण भूकंप की तीव्रता से अलग होता है और किसी भी भूकंप का परिमाण उस भूकंप द्वारा मुफ्त की गई ऊर्जा की माप होती है| अर्थात किसी भूकंप ने कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त की है उस मात्रा को हम भूकंप का परिमाण कहते हैं|
भूकंप का परिमाण मुख्यतः भूकंप की तरंगों के आयाम, त्वरण, आवृत्ति एवं अन्य कई बातों पर निर्धारित किया जाता है| भूकंप के परिमाण को हम रिक्टर पैमाने पर मापाते हैं| रिक्टर पैमाने का आविष्कार चार्ल्स ऍफ़ रिक्टर ने सन 1935 में किया था| रिक्टर पैमाने को 1965 में गुटेनबर्ग ने संशोधित किया था|
भूकंप की तीव्रता एवं उसके परिमाण में अंतर-
भूकंप की तीव्रता और परिमाण के विभिन्न माप हैं और यह एक दुसरे से काफी भिन्न हैं| भूकंप का परिमाण भूकंप के स्रोत पर उत्पन्न ऊर्जा को मापता है भूकंप के परिमाण को सिसिमोग्राफ पर निर्धारित किया जाता है। जबकि भूकंप की तीव्रता एक निश्चित स्थान पर भूकंप द्वारा उत्पादित झटकों की ताकत को मापता है। भूकंप की तीव्रता लोगों, मानव संरचनाओं (इमारतों, बांधों, पुलों आदि) और प्राकृतिक वातावरण पर प्रभाव से निर्धारित होती है।
भूकंप आने के पूर्व के लक्षण-
भूकंप का पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है| किंतु कुछ अप्रत्याशित एवं असामान्य प्राकृतिक- जैविक व्यवहार एवं घटनाओं के द्वारा कुछ लक्ष्य अवश्य प्रतीत होने लगते हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है-
- भूकंप से पूर्व पृथ्वी की रेडियोधर्मिता में हुई वृद्धि एवं असामान्य गैसों के निकलने से वातावरण में कुछ परिवर्तन हो सकता है| इससे विपदा की आशंका की जा सकती है|
- जलीय स्रोतों तथा कुआं का जल गंदा होने लगता है|
- संवेदनशील प्राणियों जैसे- कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा पक्षी अचानक उत्प्रेरित होने लगते हैं तथा अप्रत्याशित व्यवहार करने लगते हैं|
- भूकंप आने के पूर्व प्रारंभिक अवस्था में भवन के दरवाजे तथा क्रिया धीरे-धीरे खटखटाने लगती हैं| बर्तन, चारपाई, मेज, फूलदान आदि में कंपन होने लगता है| मंदिरों तथा गिरजाघरों की घंटियां बजने लगती है|
भूकंप से पूर्व सावधानियां-
- चेतावनी जारी होते ही भवन को छोड़कर मैदान में आ जाए|
- जोखिम से बचने के लिए विशेषज्ञों का परामर्श|
- ऊपर लगी हुई वस्तुएं हटा दें|
- कमजोर दीवारों को सहारा दें|
- दीवारों, पेड़ों तथा खंभों के पास में खड़े हैं
भूकंप के समय सावधानियां-
- डरिए नहीं, शांति से काम लीजिए|
- जहां है, वहीं खड़े रहिए, किंतु दीवारों, पेड़ों या खंभों का सहारा ना लें|
- चलती कार में हो तो सड़क के एक किनारे बैठ जाइए| पुल या सुरंग पार ना करें|
- बिजली बंद कर दे| गैस पाइप को बंद कर सिलेंडर को सील कर दें|
भूकंप के बाद क्या करें?
- गैस सिलेंडर बंद रखें| आग न जलाएं|
- परिवार के सदस्यों खासकर वृद्ध तथा बच्चों की देखभाल करें|
- रेडियो और टीवी बंद ना करें| आपातकालीन घोषणाएं सुनते रहे|
- छतिग्रस्त ढाचोंसे दूर रहे|
- बाद में आने वाले झटको से सचेत रहें|
भूकंप की दृष्टि से भारत का विभाजन-
भारत सरकार ने नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा BMTPC के सहयोग से प्रकाशित घातकता मानचित्रावली में संपूर्ण भारत को भूकम्पीय की दृष्टि से चार भागों में विभाजित किया गया है–
जोन 2- इसके अंतर्गत तमिलनाडु, उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा तथा प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक भाग आते हैं|
जोन 3- उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार|
जोन 4- जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का उत्तरी मैदानी भाग तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है|
जोन 5- हिमालय पर्वत श्रेणी, नेपाल, बिहार- सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य तथा कच्छ प्रायद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस जोन के अंतर्गत सम्मिलित है|
Related Articales
Recently Posted
-
भगवान गौतम बुद्ध जीवन परिचय | Gautam Buddha in Hindi
December 15, 2022. -
कार्बन के अपररूप Allotropes of Carbon in Hindi
November 5, 2022. -
मिश्र धातु किसे कहते हैं? उपयोग, नाम, गुण Alloy in Hindi
July 27, 2022. -
गलनांक किसे कहते हैं? परिभाषा, उदाहरण Melting Point in Hindi
July 20, 2022. -
परिमाप किसे कहते हैं? Perimeter in Hindi
July 19, 2022.